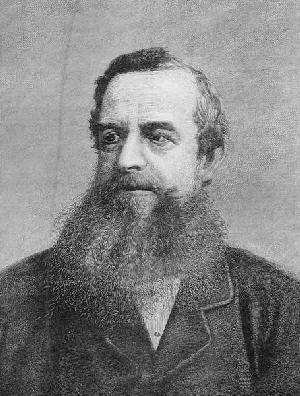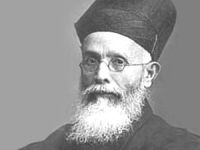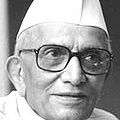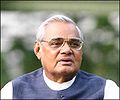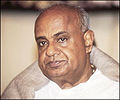"रात 12 बजे जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता पाने के
लिए जागेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ है, जब हम पुराने युग से नए
युग की ओर कदम बढ़ाएंगे... भारत दोबारा अपनी पहचान बनाएगा।" -
पंडित जवाहरलाल नेहरू (भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 1947 के अवसर पर)
यह एक देश भक्ति से भरा हुआ हृदय था, जिसमें आज़ादी के लिए प्यार और
हमारी प्यारी मातृभूमि के लिए अमर समर्पण था जो 200 साल तक अँग्रेज़ों के
राज के अधीन रहने के पर भी बना रहा और हमें अँग्रेज़ों से आज़ादी मिली।
15 अगस्त 1947, वह दिन था जब भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली और इस
प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई जब भारत के मुक्त राष्ट्र के रूप में
उठा। स्वतंत्रता दिवस के दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत के जन्म
का आयोजन किया जाता है और भारतीय इतिहास में इस दिन का अत्यंत महत्व है।
भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में अनेक अध्याय जुड़े हैं जो
1857 की क्रांति
से लेकर जलियाँवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन से लेकर नमक सत्याग्रह तक
अनेक हैं। भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है जिसमें अनेक राष्ट्रीय और
क्षेत्रीय अभियान हुए और इसमें उपयोग किए गए दो प्रमुख अस्त्र थे सत्य और
अहिंसा।
हमारी स्वतंत्रता के संघर्ष में भारत के राजनैतिक संगठनों के व्यापक
रंग, उनकी दर्शन धारा और आंदोलन शामिल हैं जो एक महान कारण के लिए एक साथ
मिलकर चले और ब्रिटिश उप-निवेश साम्राज्य का अंत हुआ और एक स्वतंत्र
राष्ट्र का जन्म हुआ।
यह दिन हमारी आज़ादी का जश्न मनाने और उस सभी शहीदों को श्रद्धांजलि
देने का अवसर जिन्होंने इस महान कारण के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीयता, भाई-चारे
और निष्ठा की भावना भर जाती है।
अनेकानेक आयोजन
स्वतंत्रता दिवस को पूरी निष्ठा, गहरे समर्पण और अपार देश भक्ति के साथ
पूरे देश में मनाया जाता है। स्कूलों और कालेजों में यह दिन सांस्कृतिक
गतिविधियों, कवायद और ध्वज आरोहण के साथ मनाया जाता है। दिल्ली में
प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और इसके बाद राष्ट्र गान
गाया जाता है। वे राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं और पिछले एक वर्ष के
दौरान देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं तथा आगे आने वाले समय के लिए
विकास का आह्वान करते हैं। इसके साथ वे आज़ादी के संघर्ष में शहीद हुए
नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान पर
अभिवादन करते हैं।
एक अत्यंत रोचक गतिविधि जो स्वतंत्रता दिवस के साथ जुड़ी हुई है, वह
है पतंग उड़ाना, जिसे आज़ादी और स्वतंत्रता का संकेत कहा जाता है।
स्वतंत्रता दिवस (
अंग्रेज़ी:
Independence Day)
ऐसा दिन है जब हम अपने महान राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों
को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने विदेशी नियंत्रण से
भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक बलिदान दिए और अपने जीवन न्यौछावर कर दिए।
15 अगस्त 1947 को भारत के निवासियों ने लाखों कुर्बानियां देकर
ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। यह राष्ट्रीय पर्व भारत के गौरव का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को सरकारी बिल्डिंगों पर
तिरंगा झण्डा फहराया जाता है तथा रौशनी की जाती है।
प्रधानमंत्री प्रातः 7 बजे
लाल क़िले
पर झण्डा लहराते हैं और अपने देशवासियों को अपने देश की नीति पर भाषण देते
हैं। हज़ारों लोग उनका भाषण सुनने के लिए लाल क़िले पर जाते हैं। स्कूलों
में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और बच्चों में मिठाईयाँ भी बाँटी
जाती हैं। 14 अगस्त को रात्रि 8 बजे
राष्ट्रपति अपने देश वासियों को सन्देश देते हैं, जिसका रेडियो तथा
टेलीविज़न पर प्रसारण किया जाता है।
सन
1857 के
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारम्भ
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रारम्भ किया और अपने प्राणों को
भारत माता पर
मंगल पांडे ने न्यौछावर किया और देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गयी जिसमें
झांसी की
रानी लक्ष्मीबाई,
तात्या टोपे,
नाना साहेब, '
सरफ़रोशी की तमन्ना' लिए
रामप्रसाद बिस्मिल,
अशफ़ाक,
चंद्रशेखर आज़ाद,
भगत सिंह,
राजगुरु,
सुखदेव आदि देश के लिए शहीद हो गए।
तिलक ने
स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का सिंहनाद किया और
सुभाष चंद्र बोस ने कहा -
तुम मुझे ख़ून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।
'अहिंसा' और 'असहयोग' लेकर महात्मा गाँधी और ग़ुलामी की जंज़ीरों को तोड़ने के लिए 'लौह पुरुष' सरदार पटेल
जैसे महापुरुषों ने कमर कस ली। 90 वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 15 अगस्त
1947 को 'भारत को स्वतंत्रता' का वरदान मिला। भारत की आज़ादी का संग्राम
बल से नहीं वरन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर विजित किया गया।
इतिहास में स्वतंत्रता के संघर्ष का एक अनोखा और अनूठा अभियान था जिसे
विश्व भर में प्रशंसा मिली।
इतिहास
मई 1857 में
दिल्ली के कुछ
समाचार पत्रों में यह भविष्यवाणी छपी कि
प्लासी के युद्ध के पश्चात्
23 जून
1757 ई. को भारत में जो अंग्रेज़ी राज्य स्थापित हुआ था वह 23 जून 1857 ई.
तक समाप्त हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सारे देश में फैल गई और लोगों में
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जोश की लहर दौड़ गई। इसके अतिरिक्त 1856 ई.
में
लार्ड कैनिंग
ने सामान्य भर्ती क़ानून पास किया। जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को यह
लिखकर देना होता था कि सरकार जहाँ कहीं भी उन्हें युद्ध करने के लिए भेजेगी
वह वहीं पर चले जाएँगे। इससे भारतीय सैनिकों में असाधारण असन्तोष फैल गया।
कम्पनी की सेना में उस समय तीन लाख सैनिक थे, जिनमें से केवल पाँच हज़ार
ही यूरोपियन थे। बाकी सब अर्थात् यूरोपियन सैनिकों से 6 गुनाह भारतीय सैनिक
थे।
[1]
सिपाही क्रांति
जब देश में चारों ओर असन्तोष का वातावरण था, तो अंग्रेज़ी सरकार ने
सैनिकों को पुरानी बन्दूकों के स्थान पर नई राइफलें देने का निश्चय किया।
इन राइफलों के कारतूस में
सूअर तथा
गाय
की चर्बी प्रयुक्त की जाती थी और सैनिकों को राइफलों में गोली भरने के लिए
इन कारतूसों के सिरे को अपने दाँतों से काटना पड़ता था। इससे
हिन्दू और
मुसलमान सैनिक भड़क उठे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेज़ सरकार उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है। इसलिए जब
मेरठ
के सैनिकों में ये कारतूस बाँटे गए तो 85 सैनिकों ने उनका प्रयोग करने से
इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें कठोर दण्ड देकर बन्दीगृह में डाल दिया गया।
सरकार के इस व्यवहार पर भारतीय सैनिकों ने 10 मई, 1857 के दिन "हर–हर
महादेव, मारो फिरंगी को" का नारा लगाते हुए विद्रोह कर दिया।
तत्पश्चात् उन्होंने जेल को तोड़कर अपने साथियों को रिहा करवा लिया और नगर में रहने वाले
अंग्रेज़ नर–नारियों का वध कर दिया। अगले दिन वे बहुत बड़ी संख्या में
दिल्ली की ओर चल पड़े और मुग़ल सम्राट
बहादुरशाह
की जय का नारा लगाते हुए दिल्ली में दाख़िल हुए। बहादुरशाह ने विद्रोह का
नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और सरकारी इमारतों पर मुग़ल ध्वज लहराया
गया।
दिल्ली में रहने वाले अंग्रेज़ों का वध कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। इसी बीच
लखनऊ,
अलीगढ़,
कानपुर,
बनारस,
रूहेलखण्ड
आदि कई स्थानों में भी विद्रोह उठ खड़े हुए और इन दिशाओं से भी भारतीय
सैनिक दिल्ली पहुँच गए। उस समय अंग्रेज़ी सेना दिल्ली में नहीं थी। इसलिए
भारतीय सैनिकों ने आसानी से दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। विद्रोहियों ने 200
अंग्रेज़ों को गोली से उड़ा दिया।
इस विद्रोह में जिन नेताओं ने अपनी–अपनी देशभक्ति तथा वीरता का परिचय दिया, उनमें शहीद
मंगल पाण्डे,
नाना साहब,
झाँसी की रानी,
तात्या टोपे, कुँवर सिंह, अजीम उल्ला ख़ाँ और
सम्राट बहादुरशाह के नाम उल्लेखनीय हैं। नाना साहब ने
कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ सेनापति व्हीलर को पराजित करके
दुर्ग को अपने क़ब्ज़े में ले लिया।
लखनऊ में भी कई दिनों तक विद्रोह चलता रहा और चीफ़ कमिश्नर सर हेनरी लोटस को मौत के घाट उतार दिया।
बनारस,
इलाहाबाद,
बरेली तथा
शाहजहाँपुर में भी काफ़ी हलचल रही और हज़ारों लोगों का रक्तपात हुआ। मध्य
भारत में
प्लासी तथा
ग्वालियर विद्रोह के प्रमुख केन्द्र बने रहे।
झाँसी की महारानी
लक्ष्मीबाई
तथा उनके सैनिकों ने स्थानीय दुर्ग में अंग्रेज़ों का डट कर मुक़ाबला
किया। काल्पी तथा ग्वालियर में भी भयंकर युद्ध लड़े गए। तात्या टोपे तथा
अन्य कुछ वीरों ने भी इस विद्रोह में बढ़–चढ़ कर भाग लिया। परन्तु झाँसी की
रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के इस प्रथम संग्राम में वीरगति को प्राप्त
हुई। इससे भारतीय विद्रोहियों का साहस टूट गया और मध्य भारत पर अंग्रेज़ों
का क़ब्ज़ा हो गया।
[1]
गुरिल्ला युद्ध प्रणाली
बिहार
में कुँवरसिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और 80
वर्ष की उम्र में भी शत्रुओं से लड़ते रहे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध
प्रणाली को अपनाया और अपने भाई अमरसिंह तथा मित्र निशानसिंह के सहयोग से
अंग्रेज़ सेनापति को हराया। उन्होंने अपनी राजधानी जगदीशपुर को पुनः
प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके भाई ने संघर्ष जारी रखा। गवर्नर
जनरल कैनिंग ने विद्रोह को दबाने के लिए
बम्बई,
मद्रास,
पंजाब
और भारतीय रियासतों से सहायता माँगी और हिन्दू मुसलमानों में फूट डलवाने
के लिए अफवाहें फैलाईं तथा गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की। तत्पश्चात्
हैदराबाद,
ग्वालियर,
पटियाला,
नाभा, जीन्द,
नेपाल
आदि कई रियासतों से सहायता मिलने पर तीन अंग्रेज़ सेनापतियों हेनरी, बरनाई
तथा निकलसन ने दिल्ली को चारों तरफ़ से घेर लिया परन्तु तीन मास तक दिल्ली
को अपने अधिकार में नहीं ले सके। अन्त में जनरल निकलसन ने एक घमासान युद्ध
के पश्चात् दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार फिर से दिल्ली पर
अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। मुग़ल सम्राट
बहादुरशाह ज़फ़र को बन्दी बनाकर रंगून (अब
यांगून)
भेज दिया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि भारतीयों का यह प्रयत्न
सफल नहीं हुआ, तो भी सन् 1857 का यह विद्रोह एक व्यापक विद्रोह था, जिसमें
भारतीय जनता के सभी वर्गों ने भाग लिया। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जिसका
उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
[1]
"इसीलिए 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।"
ईस्ट इंडिया कम्पनी का ख़ात्मा
1857 के विद्रोह ने अंग्रेज़ों के शासन प्रबन्ध की त्रुटियों का भांडा फोड़ दिया। इसलिए विद्रोह के शीघ्र पश्चात् ही
इंग्लैण्ड के राजा ने
ईस्ट इंडिया कम्पनी को ख़त्म करके भारतीय राज्य की बागडोर अपने हाथ में सम्भाल ली। सन्
1880 ई में गलैडस्टोन इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री बना। उसने
लार्ड रिपन
को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। यद्यपि 1857 से 1880 तक कैनिंग,
मेओ, लैटिन आदि कई गवर्नर जनरल भारत में शासन करते रहे, परन्तु जो सम्मान
लार्ड रिपन को प्राप्त हुआ वह इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। उसने
भारतीयों की उन्नति तथा कल्याण के लिए जो कार्य किए उनका उदाहरण मिलना कठिन
है। उसे अपने कई प्रशासनिक कार्यों के लिए अपने देशवासियों के विरोध का
सामना करना पड़ा, परन्तु उसने उनकी तनिक भी परवाह नहीं की।
[1]
लार्ड रिपन

मुख्य लेख :
लॉर्ड रिपन
लार्ड रिपन ने भारत में हर दस वर्ष में जनगणना करने का नियम बनाया और
सन् 1881 में पहली बार गणना कराई, जोकि अब तक हर दस साल के बाद की जाती है।
1882 ई. में लार्ड रिपन ने कई सुधार किए। उसने म्यूनिसिपल बोर्ड तथा
शिक्षा में सुधार किया। वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया। केन्द्रीय
सूची में अफ़ीम, रेल, डाकघर, नमक टैक्सटाइल आदि साधन रखे गए। प्रान्तीय
सूची में शिक्षा,
पुलिस,
जेल, प्रेस, तथा सार्वजनिक कार्य रखे गए। तीसरी सूची में भूमिकर, जंगल
स्टैम्प कर आदि रखे गए, इन मुद्दों के द्वारा प्राप्त आय को केन्द्रीय
सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में बाँटा गया। लार्ड रिपन ने सारे देश में
स्थानीय बोर्डों का जाल बिछा दिया और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा
दी।
लार्ड रिपन के आने से पहले लार्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया
था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अख़बारों पर कठोर
प्रतिबन्ध लगा दिए थे। भारतीय जनता ने इस एक्ट को 'गला घोंटू एक्ट' कहा था।
लार्ड रिपन ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया और भारतीय भाषाओं में छपने वाले
अख़बारों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अब वे भी अंग्रेज़ी भाषाओं में
छपने वाले अखबारों के बराबर हो गए। लार्ड रिपन ने शिक्षा में सुधार लाने के
लिए 21 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया। जिसका अध्यक्ष डब्लू हन्टर था।
इस कमीशन की सिफ़ारिशों पर शिक्षा में बहुत ही उन्नति हुई। इसके अतिरिक्त
लार्ड रिपन ने मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया और विदेशों से भारत में
आने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी ख़त्म कर दी। उसने फैक्ट्रियों में काम करने
वाले बच्चों के हित में नियम बनाए।
लार्ड रिपन ने सन् 1883 ई. में भारतीय कौंसिल में अलबर्ट बिल पेश किया। इस
बिल के अनुसार भारतीय जजों तथा सैशन जजों को अंग्रेज़ों के मुक़दमें सुनने
तथा उसका निर्णय देने का अधिकार दिया गया। इससे सारे अंग्रेज़ लार्ड के
विरुद्ध हो गए, परन्तु भारतीयों ने लार्ड रिपन की प्रशंसा की। इससे
अंग्रेज़ों और भारतीयों में ठन गई। अंग्रेज़ों ने भारतीय जजों को कलूटे
बाबू कहकर उनका अपमान किया। भारतीयों ने भी
कलकत्ता
के टाउन हॉल में अंग्रेज़ों को मुँहतोड़ जबाव दिया। श्री लाल मोहन घोष ने
अंग्रेज़ों को दो कोड़ी के अफ़सर कहकर उनकी खूब हँसी उड़ाई।
1883
के अलबर्ट बिल ने भारतीयों में जातियाँ स्वाभिमान को बहुत प्रबल किया और
उन्हें संगठित होने की प्रेरणा दी और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। जिसके
परिणामस्वरूप ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना
सार्वजनिक सभा कई प्रान्तीय संस्थाएँ बनीं। इन संस्थाओं ने शीघ्र ही भारत
में एक देशव्यापी संस्था बनाने का विचार किया।
इस बीच इंडियन सिविल सर्विस के रिटायर्ड सदस्य मि. ए. ओ. ह्यूम ने
कलकत्ता विश्वविद्यालय
के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भारतवासियों को
अपने नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए एक संघ बनाने की
प्रेरणा दी। ह्यूम के इस पत्र का भारतवासियों ने स्वागत किया और सन्
1884 ई. में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई और अगले वर्ष सन्
1885 ई. में इस संस्था का
बम्बई में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में
दादा भाई नोरोजी के परामर्श पर इस संस्था का नाम इंडियन नेशलन कांग्रेस रखा गया। यह संस्था
1905 तक उदारवादी नेताओं की देख–रेख में काम करती रही।
गोपाल कृष्ण गोखले,
दादा भाई नोरोजी,
फ़िरोजशाह मेहता,
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी,
पंडित मदन मोहन मालवीय इस संस्था के प्रमुख नेता थे।
सन 1905 ई में
कांग्रेस का अधिवेशन
बनारस में हुआ।
बंगाल विभाजन के कारण वातावरण बदल चुका था। इसलिए
लोकमान्य तिलक
तथा उनके समर्थकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उग्र नीति अपनाने का सुझाव
दिया। उदारवादी इस सुझाव से सहमत नहीं हुए। जिससे कांग्रेस में दो गुट बन
गए।
1906
ई में कलकत्ता के अधिवेशन में दोनों गुटों में बल परीक्षा हुई। परन्तु
दादा भाई नोरोजी के उपस्थित होने के कारण इस फूट को रोक लिया गया। कांग्रेस
का
1907 ई. में '
सूरत अधिवेशन' हुआ। इस अधिवेशन में दोनों दलों में झगड़ा हो गया और शीघ्र ही इसने दंगे का रूप धारण कर लिया। इससे कांग्रेस के दो दल बन गए-
गरम दल और
नरम दल।
[1]
लार्ड कर्ज़न

मुख्य लेख :
लॉर्ड कर्ज़न
1905 से
1919 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादियों के हाथ में रहा। उग्रवादियों के प्रमुख नेता बाल, लाल, पाल (
बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय और
विपिन चन्द्र पाल)
थे। लाला लाजपत राय ने उदारवादियों की नीति पर असन्तुष्ट होकर कहा था कि
हमें बीस लगातार आंदोलन करने के बाद भी रोटी के बदले पत्थर मिले। हम
अंग्रेज़ों के आगे अब और अधिक समय तक भीख नहीं माँगेंगे और न ही उनके सामने
गिड़गिड़ायेंगे।
दक्षिण अफ्रीका
में तो भारतीयों की हालत बहुत शोचनीय थी। रंगभेद की दृष्टि के कारण उन्हें
घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अस्पतालों तथा होटलों में प्रवेश
करने की अनुमति नहीं थी। बच्चे उच्च संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त नहीं कर
सकते थे। रजिस्ट्रेशन एक्ट (1907) के तहत भारतीयों को अपराधियों के तरह
दफ़्तरों में अपने नाम लिखवाने पड़ते थे और अपनी अंगुलियों की छाप देनी
पड़ती थी।
लार्ड कर्ज़न
की दमन नीति (1898 से 1905) ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। उसने
अपने भाषण में भारतीयों को बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे थे और कार्यकुशलता के
नाम पर कलकत्ता कार्पोरेशन आफिसयल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनीवर्सटी एक्ट,
कई ऐसे क़दम उठाए जिनका उद्देश्य भारतीय एकता को दुर्बल करना तथा भारतीय
भावनाओं का गला घोंटना था। 1907 ई. में बंगाल भंग सम्बन्धी घोषणा होते ही
गरम दल सक्रिय हो गया। उन्होंने
दिसम्बर 1907
में बंगाल के गवर्नर की गाड़ी पर बम फैंकने का प्रयत्न किया। फिर ढाका के
मजिस्ट्रेट पर गोली चलाई। परन्तु वह बच निकला। मुजफ़्फ़पुर बम फटने से
कैनेडी तथा उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई।
पंजाब और
महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएँ होने लगीं।
[1]
ग़दर पार्टी की स्थापना

मुख्य लेख :
ग़दर पार्टी
सन्
1913 में
अमेरिका में बसने वाले भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के प्रमुख नेता
सोहनसिंह भकना,
लाला हरदयाल, बाबा बसाखा सिंह, पं. काशीराम और उधमसिंह थे। इस पार्टी के हज़ारों भारतवासी अमेरिका से भारत आए। उन्होंने
लाहौर,
फ़िरोजपुर,
अम्बाला,
मेरठ,
आगरा आदि सैनिक छावनियों में सैनिकों को विद्रोह करने की प्रेरणा दी और
25 फरवरी 1915
को गदर का दिन रखा। लेकिन कुपाल सिंह के विश्वासघात ने इस योजना को असफल
कर दिया। गदर पार्टी की तरह इंडो जर्मन मिशन ने भी टर्की और
काबुल का सहयोग प्राप्त करके भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई और अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, जिसके राष्ट्रपति
राजा महेन्द्र प्रताप
और प्रधान मंत्री बरकत अल्लाह थे। लेकिन परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण
ये देशभक्त भी सफल नहीं हो सके। सौभाग्य से दक्षिण अफ्रीका में
भारतवासियों को
महात्मा गांधी के रूप में एक ऐसा नेता मिला जिसने सब भारतवासियों को संगठित किया। उन्होंने
सत्याग्रह आंदोलन चलाया और भारतीयों पर लगाए गए क़ानून रोक दिए।
प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीयों से मदद माँगी थी और कुछ
सहूलियतें देने का वायदा किया था। भारतीयों ने दिलोंजान से अंग्रेज़ों की
मदद की। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने जो सुविधा
दी वह ना के बराबर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन रियाययों की निन्दा
की। सरकार ने हिन्दुस्तानियों को दबाने के लिए रोलट एक्ट पास किया। इस एक्ट
के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुक़दमा चलाए बन्दी बना सकती थी।
उसे अपने पक्ष में अलील, दलील तथा वक़ील का अधिकार भी नहीं था। महात्मा
गांधी ने
13 मार्च 1919 को रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। परन्तु दुर्भाग्य से आंदोलन के दौरान
अहमद नगर,
दिल्ली और
पंजाब में उपद्रव हो गए, जिसके कारण
महात्मा गाँधी को आंदोलन स्थगित करना पड़ा।
10 अप्रैल 1919 को पंजाब के डिप्टी कमिश्नर ने सत्यपाल और डॉ. किचलू को अपनी कोठी पर बुलाकर अचानक बन्दी बना लिया। 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग़ से पच्चीस हज़ार नागरिक सभा करने के लिए एकत्रित हुए। अंग्रेज़
जनरल डायर
ने उनको घेर कर गोली चलवा दी और हज़ारों निहत्थे लोग मौत के घाट उतार दिए।
इस घटना के बाद भारतवासियों ने फ़ैसला किया कि अंग्रेज़ों को भारत पर
हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है।
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई।
पंजाब में
भगतसिंह और उनके साथियों ने नौजवान भारत की नींव डाली। परन्तु ये देशभक्त भी सफल नहीं हो सके और
23 मार्च 1930 को भगत सिंह,
सुखदेव और
राजगुरु को अंग्रेज़ों ने फ़ाँसी पर चढ़ा दिया।
[1]
गांधी जी के आंदोलन
बम्बई प्रान्त में जितेन्द्रनाथ ने 61 दिन भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग दिए। गांधी ने
नमक
क़ानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च किया। क़ानून तोड़ने पर अंग्रेज़ों ने
गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन देश में आंदोलन ज़ोर पकड़ गया, इसलिए
गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने तीन बार
लन्दन में गोल मेज कांफ़्रेन्स बुलाई, लेकिन गांधीजी हर बार निराश ही वापस लौटे।
3 सितम्बर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया।
8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ। उसमें "
भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास हुआ।
पंडित मोतीलाल नेहरू तथा
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। अंग्रेज़ सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। इस बीच नेताजी
सुभाष चन्द्र बोस ने
भारत से बाहर रहकर भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न किया। उनका विचार था कि द्वितीय विश्वयुद्ध का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने
आज़ाद हिन्द फ़ौज
की स्थापना की। और "दिल्ली चलो" का नारा दिया। लेकिन नेताजी किसी दुर्घटना
में मारे गए, इसलिए यह आंदोलन भी असफल हो गया। तत्पश्चात्
18 फरवरी 1946
को बम्बई में सैनिक विद्रोह उठ खड़े हुए। सैनिकों ने अपनी बैरकों से
निकलकर अंग्रेज़ सैनिकों पर धावा बोल दिया और पाँच दिन तक अंग्रेज़ी
सैनिकों को मौत के घाट उतारते रहे। अन्त में अंग्रेज़ों को यह बात स्पष्ट
हो गई कि अब वे भारत को अधिक समय तक अपना ग़ुलाम बनाकर नहीं रख सकते।
इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री किलैमण्ट एटली ने भारत समस्या सुलझाने के लिए
23 मार्च 1946
को तीन अधिकारियों—पैथिक लारेन्स, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए. बी. एलैज़ेण्डर
को भारत भेजा। उन्होंने भारतीय नेताओं से तथा वायसराय से बातचीत की।
14 अगस्त 1946 ई. को वायसराय ने केन्द्र में अन्तरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया। परन्तु
मुस्लिम लीग ने
पाकिस्तान
की माँग की और सीधी कार्यवाही के मार्ग को अपनाया। 16 अगस्त को कलकत्ते
में काफ़ी खून–ख़राबा हुआ, हज़ारों लोग मारे गए तथा करोड़ों की सम्पत्ति
नष्ट कर दी गई।
फरवरी 1947
को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने एक ब्यान दिया, जिसके अनुसार हिन्दुस्तान
को 1948 में स्वतंत्र करने की घोषणा की। इस ब्यान के साथ भारत के वायसराय
लार्ड बावेल को वापस इंग्लैण्ड बुला लिया गया और उसकी जगह पर
लार्ड माउण्टबेटन
को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। लार्ड माउण्टबेटन ने भारत का बँटवारा करना
ही बेहतर समझा। कांग्रेसी नेताओं ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और
4 जुलाई 1947
को इंग्लैण्ड की संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 16
जुलाई 1947 को संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पास कर दिया और 18
जुलाई 1947 को इंग्लैण्ड के बादशाह ने भी अपनी स्वीकृति दे दी।
[1]
स्वतंत्रता की राह
20वीं शताब्दी में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों ने
महात्मा गाँधी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने हिंसापूर्ण संघर्ष के विपरीत '
सविनय अवज्ञा अहिंसा आंदोलन'
को सशक्त समर्थन दिया। उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए मार्च,
प्रार्थना सभाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को
प्रोत्साहन देना आदि अचूक हथियार थे। इन रास्तों को भारतीय जनता ने समर्थन
दिया और स्थानीय अभियान 'राष्ट्रीय आंदोलन' में बदल गए। इनमें से कुछ
मुख्य आयोजन - '
असहयोग आंदोलन', '
दांडी मार्च', 'नागरिक अवज्ञा अभियान' और '
भारत छोड़ो आंदोलन'
थे। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब उपनिवेशवादी शक्तियों के
नियंत्रण में नहीं रहेगा और ब्रिटिश शासकों ने भारतीय नेताओं की मांग को
मान लिया। यह निर्णय लिया गया कि यह अधिकार भारत को सौंप दिया जाए और 15
अगस्त 1947 को भारत को यह अधिकार सौंप दिया गया।
भारतवर्ष का विभाजन
15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष हिन्दुस्तान तथा
पाकिस्तान दो हिस्सों में बँटकर स्वतंत्र हो गया।
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल क़िले पर
तिरंगा
झण्डा फहराया। उसी दिन से हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता
है। सरकारी बिल्डिंगों पर तिरंगा झण्डा फहराया जाता है तथा रौशनी की जाती
है। प्रधानमंत्री प्रातः 7 बजे लाल क़िले पर झण्डा लहराते हैं और अपने
देशवासियों को अपने देश की नीति पर भाषण देते हैं। हज़ारों लोग उनका भाषण
सुनने के लिए लाल क़िले पर जाते हैं। स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया
जाता है और बच्चों में मिठाईयाँ भी बाँटी जाती हैं। 14 अगस्त को रात्रि 8
बजे
राष्ट्रपति अपने देश वासियों को सन्देश देते हैं, जिसका रेडियो तथा
टेलीविज़न पर प्रसारण किया जाता है।
[1]
स्वतंत्र भारत की घोषणा
14 अगस्त 1947 को रात को 11.00 बजे संघटक सभा द्वारा भारत की
स्वतंत्रता को मनाने की एक बैठक आरंभ हुई, जिसमें अधिकार प्रदान किए जा
रहे थे। जैसे ही घड़ी में रात के 12.00 बजे भारत को आज़ादी मिल गई और भारत
एक स्वतंत्र देश बन गया। तत्कालीन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण 'नियति के साथ भेंट' दिया।
'“जैसे ही मध्य रात्रि हुई, और जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग
रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। एक ऐसा पल आता है जो इतिहास में
दुर्लभ है, जब हम पुराने युग से नए युग की ओर जाते हैं. . . क्या हम इस
अवसर का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त बहादुर और बुद्धिमान हैं और हम भविष्य
की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?”' - पंडित जवाहरलाल नेहरू
इसके बाद
तिरंगा झण्डा फहराया गया और
लाल क़िले की प्राचीर से
राष्ट्रीय गान गाया गया।
आयोजन
स्वतंत्रता दिवस समीप आते ही चारों ओर खुशियां फैल जाती है। सभी प्रमुख
शासकीय भवनों को रोशनी से सजाया जाता है। तिरंगा झण्डा घरों तथा अन्य
भवनों पर फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त एक राष्ट्रीय अवकाश
है, इस दिन का अवकाश प्रत्येक नागरिक को बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों
द्वारा किए गए बलिदान को याद करके मनाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के एक
सप्ताह पहले से ही विशेष प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा
देश भक्ति की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता है। रेडियो स्टेशनों और
टेलीविज़न चैनलों पर इस विषय से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।
शहीदों की कहानियों के बारे में फिल्में दिखाई जाती है और राष्ट्रीय
भावना से संबंधित कहानियां और रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं।
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या
राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के
नाम संदेश प्रसारित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन लाल क़िले से तिरंगा
झण्डा फहराया जाता है। राज्य स्तर पर विशेष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम
आयोजित किए जाते हैं, जिसमें झण्डा फहराने के आयोजन, मार्च पास्ट और
सांस्कृतिक आयोजन शामिल हैं। इन आयोजनों को राज्यों की राजधानियों में
आयोजित किया जाता है और मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते
हैं। छोटे पैमानों पर शैक्षिक संस्थानों, आवास संघों, सांस्कृतिक
केन्द्रों और राजनीतिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक पतंग
स्वतंत्रता दिवस का एक और प्रतीक
पतंग
उड़ाने का खेल है। आकाश में ढेर सारी पतंगें दिखाई देती हैं जो लोग अपनी
अपनी छतों से उड़ा कर भारत की स्वतंत्रता का समारोह मनाते हैं। अलग अलग
प्रकार, आकार और रंगों की पतंगों तथा तिरंगे बाज़ार में उपलब्ध हैं। इस
दिन पतंग उड़ाकर अपने संघर्ष के कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है।
प्रभातफेरी
स्कूलों और संस्थाओं द्वारा प्रात: ही प्रभातफेरी निकाली जाती हैं
जिनमें बच्चे, युवक और बूढ़े देशभक्ति के गाने गाते हैं और उन वीरों की याद
में नुक्क्ड़ नाटक और प्रशस्ति गान करते हैं।
देशभक्ति का प्रदर्शन
भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है और यह दुनिया का सबसे
बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ के नागरिक देश को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की
वचनबद्धता रखते हैं जहां तक इसके संस्थापकों ने इसे पहुंचाने की कल्पना
की। जैसे ही आसमान में तिरंगा लहराता है, प्रत्येक नागरिक देश की शान को
बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करने का वचन देता है और भारत को एक ऐसा
राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने का प्रण लेता है जो मानवीय मूल्यों
के लिए सदैव अटल है।
लाल क़िले पर तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री
लाल क़िले पर तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री
जश्न-ए-आजादी के सिलसिले में लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा 17 बार
तिरंगा लहराने का अवसर प्रथम
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला, वहीं उनकी पुत्री
इंदिरा गाँधी ने भी राष्ट्रीय राजधानी स्थित सत्रहवीं शताब्दी की इस धरोहर पर 16 बार राष्ट्रध्वज फहराया। नेहरू ने आजादी के बाद सबसे पहले
15 अगस्त,
1947 को लाल किले पर झंडा फहराया और अपना बहुचर्चित संबोधन दिया। नेहरू जी
27 मई,
1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने लगातार 17 स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। आजाद भारत के इतिहास में
गुलजारी लाल नंदा और
चंद्रशेखर
ऐसे नेता रहे जो प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर
तिरंगा फहराने का एक भी बार मौका नहीं मिल सका। नेहरू के निधन के बाद 27
मई,
1964 को नंदा प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वर्ष 15 अगस्त आने से पहले ही
9 जून, 1964 को वह पद से हट गए और उनकी जगह
लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। नंदा 11 से
24 जनवरी,
1966 के बीच भी प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसी तरह चंद्रशेखर
10 नवंबर,
1990 को
प्रधानमंत्री, बने लेकिन
1991 के स्वतंत्रता दिवस से पहले ही उस वर्ष
21 जून को पद से हट गए।
लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद नंदा कुछ दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन बाद में 24 जनवरी, 1966 को नेहरू की पुत्री
इंदिरा गाँधी
ने सत्ता की बागडोर संभाली। नेहरू के बाद सबसे अधिक बार जिस प्रधानमंत्री
ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, वह इंदिरा ही रहीं। इंदिरा 1966 से लेकर
24 मार्च,
1977 तक और फिर
14 जनवरी,
1980 से लेकर
31 अक्टूबर,
1984
तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल में
उन्होंने 11 बार और दूसरे कार्यकाल में पाँच बार लाल किले पर झंडा फहराया।
स्वतंत्रता दिवस पर सबसे कम बार राष्ट्रध्वज फहराने का मौका
चौधरी चरण सिंह-28 जुलाई,
1979 से
14 जनवरी,
1980;
विश्वनाथ प्रताप सिंह-2 दिसंबर,
1989 से
10 नवंबर,
1990;
एच. डी. देवगौड़ा-1 जून,
1996 से
21 अप्रैल,
1997 और
इंद्र कुमार गुजराल-21 अप्रैल,
1997 से लेकर
28 नवंबर, 1997 को मिला। इन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक-एक बार
15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराया।
9 जून, 1964 से लेकर 11 जनवरी, 1966 तक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर
शास्त्री और 24 मार्च, 1977 से लेकर 28 जुलाई, 1979 तक प्रधानमंत्री रहे
मोरारजी देसाई को दो- दो बार यह सम्मान हासिल हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर पाँच
या उससे अधिक बार तिरंगा फहराने का मौका नेहरू और इंदिरा गाँधी के अलावा
राजीव गाँधी, पी. वी. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह को मिला है। राजीव 31 अक्टूबर, 1984 से लेकर एक दिसंबर, 1989
तक और नरसिंह राव 21 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। दोनों
को पाँच-पाँच बार ध्वज फहराने का मौका मिला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
की सरकार का नेतृत्व कर चुके अटल बिहारी वाजपेयी जब 19 मार्च, 1998 से लेकर
22 मई, 2004 के बीच प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने कुल छह बार लाल किले की
प्राचीर से तिरंगा फहराया। इससे पहले वह एक जून 1996, को भी
प्रधानमंत्री बने, लेकिन 21 अप्रैल, 1997 को ही उन्हें पद से हटना पड़ा था। वर्ष
2004
के आम चुनाव में राजग की हार के बाद संप्रग सत्ता में आया और मनमोहन सिंह
ने 22 मई, 2004 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें छ: बार तिरंगा फहराने
का सौभाग्य मिला।
[2]
 With just a week left for the SSC CGL Tier-I 2016 exam to
flag off, you all must be in the last leg of your preparation. As per
the new exam pattern, the CGL Tier-I exam will be a Computer Based Test
(CBT). Since this is the first time that SSC is conducting an online
exam, you all must be hoping that it turns fruitful for you.
With just a week left for the SSC CGL Tier-I 2016 exam to
flag off, you all must be in the last leg of your preparation. As per
the new exam pattern, the CGL Tier-I exam will be a Computer Based Test
(CBT). Since this is the first time that SSC is conducting an online
exam, you all must be hoping that it turns fruitful for you.